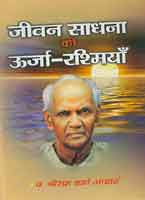|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> देव संस्कृति की गौरवगरिमा अक्षुण्ण रहे देव संस्कृति की गौरवगरिमा अक्षुण्ण रहेश्रीराम शर्मा आचार्य
|
402 पाठक हैं |
||||||
देव संस्कृति की गौरवगरिमा.....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारतीय संस्कृति उत्कृष्टता का केंद्र बिंदु
भारत एक देश नहीं, मानवी उत्कृष्टता एवं संस्कृति का उद्गम केंद्र है।
हिमालय के शिखरों पर जमा बर्फ जल धारा बनकर बहता है, अपनी शीतलता और
पवित्रता से एक सुविस्तृत भू -भाग को सरसता एवं हरीतिमा युक्त कर देता है।
भारतवर्ष धर्म और अध्यात्म का उदयाचल है, जहाँ से सूर्य उगता और सारे
भूमंडल को आलोक से भर देता है। प्रकारांतर से यह आलोक ही जीवन है जिसके
सहारे वनस्पतियाँ उगतीं, घटाएँ बरसतीं, और प्राणियों में सजीवता की हलचलें
होती हैं। ‘डार्विन’ ने अपने प्रतिपादन में मानव को
बंदर की
औलाद कहा है। सचमुच यही स्थिति व्यवहार में रही होती यदि नीतिमत्ता,
मर्यादा, सामाजिकता, सहकारिता, उदारता जैसे सद्गुण उसमें विकसित न हुए
होते।
बीज में वृक्ष की समस्त विशेषताएँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं, किंतु वे स्वतः विकसित नहीं हो पातीं। वे प्रसुप्त ही पड़ी रहतीं, यदि अनुकूल परिस्थितियाँ न मिलतीं। प्रयत्नपूर्वक उसे अंकुरित, विकसित करके विशाल बनने की स्थिति तक पहुँचाना पड़ता है। मनुष्य के संबंध में भी तकरीबन यही बात है। सृष्टा ने उसे सृजा तो अपने हाथों से ही है एवं असीम संभावनाओं से परिपूर्ण भी बनाया है, पर साथ ही इतनी कमी भी छोड़ी है कि विकास के प्रयत्न बन पड़ें, तो ही समुन्नत स्तर तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। प्रत्यक्ष है कि जिन्हें सुंस्कारिता का वातावरण मिला वे प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गए। जिन्हें उससे वंचित रहना पड़ा वे अभी भी अन्य प्राणियों की तरह रहते और पिछड़ी परिस्थितियों में समय गुजारते हैं। इस प्रगतिशीलता के युग में भी ऐसे वनमानुषों की कमी नहीं, जिन्हें बंदर की औलाद ही नहीं, उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है। यह पिछड़ापन और कुछ नहीं, प्रकारांतर से संस्कृति का प्रकाश न पहुँच सकने के कारण उत्पन्न हुआ अभिशाप भर है।
अन्य धर्म प्रचलनों की तुलना हमारी संस्कृति से नहीं की जा सकती। इसे किसी वर्ग, समुदाय क्षेत्र या संप्रदाय की मान्यताओं के समर्थन में नहीं गढ़ा गया है, वरन मानव की सार्वभौम सत्ता को उत्कृष्ट एवं प्रखर बनाने वाले सिद्धांतों का समावेश करते हुए इस स्तर का बनाया गया है कि उसे हृदयंगम करने वाले आचरण में उतारने वाले देव मानवों की तरह जी सकें। आज विश्व की प्रगति की दिशा में चल रही क्रमिक गतिशीलता के पीछे जिसे दिव्य अनुदान की झांकी मिलती है उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत की देव संस्कृति का अनुदान मानते और कृतज्ञता पूर्वक शतशत नमन करते हैं।
भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति नाम मिल गया। यह एक संयोग मात्र है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष के प्रति आग्रह या पक्षपात नहीं है। यदि यह सर्वप्रथम कहीं अन्यत्र उगी-उपजी होती तो संभवतः उसे उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगता। उत्पादन कर्त्री भूमिका के साथ उसके उपार्जनों का नाम भी जुड़ जाता है। इसे प्रचलन ही कहेंगे। नागपुरी संतरे, लखनवी आम, असमी चाय, नागौरी बैल, अरबी घोड़े, मैसूरी चंदन का यह अर्थ नहीं कि वे क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहेंगे। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति मानवी- संस्कृति के रूप में ही जाना माना गया है।
संसार के महामानवों ने उसका मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया है। इतिहास के पृष्ठों पर इन तथ्यों का सुविस्तृत उल्लेख है कि इस देव संस्कृति का प्रवाह मलयज पवन की तरह समस्त संसार में बिखरा और उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में भारी योगदान दिया। किसी समय इस तत्त्वदर्शन को सर्वत्र जगद्गुरु, चक्रवर्ती धरती को स्वर्ग जैसे नामों से कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्फुरणा कहा जा सकता है।
भारतीय संस्कृति की गरिमा-संपन्नों, विद्वानों की प्रतिभा की चमत्कृति नहीं कही जा सकती, मध्यकालीन संस्कृति दबाब और प्रलोभनों के सहारे अगणित लोगों पर लदी और फैली है, किंतु देव संस्कृति के बारे में इस प्रकार उँगली उठाने की कहाँ गुंजाइश नहीं है। इसका तत्त्वदर्शन अपने आप में अद्भुत और महान है। उसे भावुक अभिव्यक्तियों में अमृत पारस, कल्प वृक्ष जैसे अलंकारिक नाम देकर सम्मानित किया जाता रहा है। अपनाने पर उपलब्ध होने वाले परिणामों और फलितार्थों की महत्ता को देखते हुए इस प्रकार की मान्यता सहज ही बनती चली गई है। श्रेष्ठता किसी वर्ग या क्षेत्र विशेष की बपौती नहीं है। उसे समस्त मानवता की सर्वमान्य गौरव गरिमा का श्रेय मिलना चाहिए और औचित्य को ग्रहण करने की सत्यानुयायी विवेकशीलता को उसे बिना किसी हिचक के मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा होता भी है। संसार भर में ऐसे विवेकवानों की भारी संख्या विद्यमान रही है, जो एक स्वर में भारत की नर्सरी में उगी और विश्व उद्यान में स्थान -स्थान पर पनपी देव संस्कृति को उत्कृष्टता की अधिष्ठात्री मानते हैं और कहते हैं कि इसके अनुसरण में हर दृष्टि से हित ही हित है।
पूर्वजों की गरिमा का श्रेय उनके वंशधरों को विशेष रूप से मिलता है, यह सर्व विदित है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि उसे दुर्गति ग्रस्त न होने देने से ही सम्मानित रूप से बनाए रहने की जिम्मेदारी भी उन्हें अन्य लोगों की तुलना में अधिक गंभीरतापूर्वक समझनी और समझानी चाहिए। श्रेष्ठता की इसलिए अवहेलना की जाए कि वह पुरातन हो चली, बुद्धि संगत नहीं है। शाश्वत सत्यों का सदा समर्थन होना चाहिए। उनके साथ अतीत का इतिहास भी जुड़ गया है। इसलिए अपेक्षाकृत उसे और भी अधिक श्रद्धा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस प्रतिपादन ने पिछले लंबे समय से मनुष्य को दिशा देने और सेवा साधना करने की प्रशस्ति पाई है। इसी दृष्टि से उस समुदाय विशेष के लिए पूर्वजों की थाती को सुरक्षित और जीवंत रखने का धर्म कर्तव्य पालन करने का विशेष दायित्व माना जाता है।
निष्पक्ष विवेक, विश्व, विवेक का कर्तव्य है कि देव संस्कति की गरिमा और उपयोगिता को बिना झिझके स्वीकारें किंतु, ऐसा करने पर निकटवर्ती लोगों का पूर्वाग्रह बुरा मानेगा। यदि ऐसा अन्यत्र न बन पड़े तो भी इन उत्तराधिकारियों को विशेष रूप से जागरूकता बरतनी चाहिए कि ऐसी महान धरोहर धूमिल न होने पाए जिसने पिछले दिनों मानवता की महान सेवा की है और जिससे भविष्य में विश्व को शांति और प्रगति में महान योगदान मिलने की संभावना है।
कोई बात कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में न उतरे, चिंतन पर छाई रहे, तो पुस्तकों में सीमाबद्ध रहने पर उपेक्षित होते-होते वह विस्मृति के गर्त में जा गिरेगी और अपना अस्तित्व गँवां देगी।
‘संस्कृति’ दर्शन व परंपरा का एक समुच्चय है। अध्यात्म और धर्म का जोड़ा है। अध्यात्म आस्था को एवं व्यवहार को कहते हैं। मान्यताएँ क्रियाकलापों में भी उतरनी चाहिए। देवसंस्कृति के अनुयायी चाहे वे भारत में बसे हों अथवा प्रवासियों के रूप में सुदूर देशों में, उनका यह कर्तव्य है कि यदि वे उसकी गरिमा को स्वीकार करते हैं तो इतना और करें कि उनके आहार-विहार प्रथा प्रचलन रीति-रिवाज, कला-सज्जा, संभाषण, शिष्टाचार आदि में भी उसकी झलक दिखा सकें।
पश्चिम को प्रगतिशील मानना हो और उनका अनुकरण करना हो तो इस तथ्य पर भी गौर करना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति को ईसाई धर्म से अधिक प्यार करते थे। गर्म देशों में रहते हुए भी ठंडे मुल्कों की पोशाक पहनने में वे अपना गौरव मानते थे। संस्कृति की अवधारणा एवं निर्वाह आत्म गौरव का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
संसार का सामान्य क्रम प्रकृति-प्रेरणा के अनुरूप चल रहा है। प्राणी समुदाय की चेष्टाएँ उसी ढर्रे में गतिशील रहती हैं। पर मनुष्य की स्थिति अन्य सभी प्राणियों से भिन्न है। यह कर्म प्रधान है, उच्चस्तरीय पुरुषार्थ संपन्न प्राणी हैं। विकास की असीम संभावना होते हुए भी मनुष्य के शरीर में वासना, मन में तृष्णा तथा अंतराल में अहंता और वातावरण में निकृष्टता, प्रचलन में पशु-प्रवृत्तियों का बाहुल्य रहने से खतरा यह बना रहता है कि मानवी गरिमा असुरता के चंगुल में फँसकर कहीं उस देवोपम सौभाग्य को दुर्भाग्य में न बदल दें। प्रगति की संभावनाओं से वह विमुख न हो जाए। आकर्षणों के जाल-जंजाल में फँसकर कहीं सुरदुर्लभ सुयोग को नरक की संरचना में न लगा बैठे।
पतनोन्मुखी प्रवाह से बचकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने तथा उन महान संभावनाओं को साकार कर सकने के लिए अभीष्ट परिणाम में साहस एवं विवेक का होना आवश्यक है। इन गुणों के सहारे एकाकी अपने बलपूते प्रगति पथ की ओर बढ़ सके इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा जो मानव के संचित कुसंस्कारों को दबाने तथा प्रसुप्त दैवी तत्त्वों को उभारने में समर्थ हो सके, यह संस्कृति कहलाती है। संस्कृति अर्थात् व्यक्तित्व को परिष्कृत तथा सुविकसित करने वाली विद्या। इसके दार्शनिक पक्ष को अध्यात्म और व्यवहार को धर्म कहते हैं। दोनों के समन्वय से परिपूर्ण स्तर की जीवन शिक्षा की व्यवस्था बनती है। चिंतन और स्वभाव में उतरकर वह जीवन विद्या मनुष्य को महान बनाती है। ऐसी विशेषताओं से सुसंपन्न मनीषियों को सांसारिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर पाते। संसार के पतनोन्मुख प्रवाह की उल्टी दिशा में वे मछली की भांति धार को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं।
बीज में वृक्ष की समस्त विशेषताएँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं, किंतु वे स्वतः विकसित नहीं हो पातीं। वे प्रसुप्त ही पड़ी रहतीं, यदि अनुकूल परिस्थितियाँ न मिलतीं। प्रयत्नपूर्वक उसे अंकुरित, विकसित करके विशाल बनने की स्थिति तक पहुँचाना पड़ता है। मनुष्य के संबंध में भी तकरीबन यही बात है। सृष्टा ने उसे सृजा तो अपने हाथों से ही है एवं असीम संभावनाओं से परिपूर्ण भी बनाया है, पर साथ ही इतनी कमी भी छोड़ी है कि विकास के प्रयत्न बन पड़ें, तो ही समुन्नत स्तर तक पहुँचने का अवसर मिलेगा। प्रत्यक्ष है कि जिन्हें सुंस्कारिता का वातावरण मिला वे प्रगति पथ पर अग्रसर होते चले गए। जिन्हें उससे वंचित रहना पड़ा वे अभी भी अन्य प्राणियों की तरह रहते और पिछड़ी परिस्थितियों में समय गुजारते हैं। इस प्रगतिशीलता के युग में भी ऐसे वनमानुषों की कमी नहीं, जिन्हें बंदर की औलाद ही नहीं, उसकी प्रत्यक्ष प्रतिकृति भी कहा जा सकता है। यह पिछड़ापन और कुछ नहीं, प्रकारांतर से संस्कृति का प्रकाश न पहुँच सकने के कारण उत्पन्न हुआ अभिशाप भर है।
अन्य धर्म प्रचलनों की तुलना हमारी संस्कृति से नहीं की जा सकती। इसे किसी वर्ग, समुदाय क्षेत्र या संप्रदाय की मान्यताओं के समर्थन में नहीं गढ़ा गया है, वरन मानव की सार्वभौम सत्ता को उत्कृष्ट एवं प्रखर बनाने वाले सिद्धांतों का समावेश करते हुए इस स्तर का बनाया गया है कि उसे हृदयंगम करने वाले आचरण में उतारने वाले देव मानवों की तरह जी सकें। आज विश्व की प्रगति की दिशा में चल रही क्रमिक गतिशीलता के पीछे जिसे दिव्य अनुदान की झांकी मिलती है उसे पर्यवेक्षक एक स्वर से भारत की देव संस्कृति का अनुदान मानते और कृतज्ञता पूर्वक शतशत नमन करते हैं।
भारत में जन्मने के कारण उसे भारतीय संस्कृति नाम मिल गया। यह एक संयोग मात्र है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष के प्रति आग्रह या पक्षपात नहीं है। यदि यह सर्वप्रथम कहीं अन्यत्र उगी-उपजी होती तो संभवतः उसे उस क्षेत्र के नाम से पुकारा जाने लगता। उत्पादन कर्त्री भूमिका के साथ उसके उपार्जनों का नाम भी जुड़ जाता है। इसे प्रचलन ही कहेंगे। नागपुरी संतरे, लखनवी आम, असमी चाय, नागौरी बैल, अरबी घोड़े, मैसूरी चंदन का यह अर्थ नहीं कि वे क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहेंगे। भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति मानवी- संस्कृति के रूप में ही जाना माना गया है।
संसार के महामानवों ने उसका मूल्यांकन इसी दृष्टि से किया है। इतिहास के पृष्ठों पर इन तथ्यों का सुविस्तृत उल्लेख है कि इस देव संस्कृति का प्रवाह मलयज पवन की तरह समस्त संसार में बिखरा और उसने बिना किसी भेदभाव के हर क्षेत्र को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने में भारी योगदान दिया। किसी समय इस तत्त्वदर्शन को सर्वत्र जगद्गुरु, चक्रवर्ती धरती को स्वर्ग जैसे नामों से कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया जाता था। इसे श्रेष्ठता के प्रति सहज श्रद्धा की स्वतः स्फुरणा कहा जा सकता है।
भारतीय संस्कृति की गरिमा-संपन्नों, विद्वानों की प्रतिभा की चमत्कृति नहीं कही जा सकती, मध्यकालीन संस्कृति दबाब और प्रलोभनों के सहारे अगणित लोगों पर लदी और फैली है, किंतु देव संस्कृति के बारे में इस प्रकार उँगली उठाने की कहाँ गुंजाइश नहीं है। इसका तत्त्वदर्शन अपने आप में अद्भुत और महान है। उसे भावुक अभिव्यक्तियों में अमृत पारस, कल्प वृक्ष जैसे अलंकारिक नाम देकर सम्मानित किया जाता रहा है। अपनाने पर उपलब्ध होने वाले परिणामों और फलितार्थों की महत्ता को देखते हुए इस प्रकार की मान्यता सहज ही बनती चली गई है। श्रेष्ठता किसी वर्ग या क्षेत्र विशेष की बपौती नहीं है। उसे समस्त मानवता की सर्वमान्य गौरव गरिमा का श्रेय मिलना चाहिए और औचित्य को ग्रहण करने की सत्यानुयायी विवेकशीलता को उसे बिना किसी हिचक के मान्यता प्रदान करनी चाहिए। ऐसा होता भी है। संसार भर में ऐसे विवेकवानों की भारी संख्या विद्यमान रही है, जो एक स्वर में भारत की नर्सरी में उगी और विश्व उद्यान में स्थान -स्थान पर पनपी देव संस्कृति को उत्कृष्टता की अधिष्ठात्री मानते हैं और कहते हैं कि इसके अनुसरण में हर दृष्टि से हित ही हित है।
पूर्वजों की गरिमा का श्रेय उनके वंशधरों को विशेष रूप से मिलता है, यह सर्व विदित है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि उसे दुर्गति ग्रस्त न होने देने से ही सम्मानित रूप से बनाए रहने की जिम्मेदारी भी उन्हें अन्य लोगों की तुलना में अधिक गंभीरतापूर्वक समझनी और समझानी चाहिए। श्रेष्ठता की इसलिए अवहेलना की जाए कि वह पुरातन हो चली, बुद्धि संगत नहीं है। शाश्वत सत्यों का सदा समर्थन होना चाहिए। उनके साथ अतीत का इतिहास भी जुड़ गया है। इसलिए अपेक्षाकृत उसे और भी अधिक श्रद्धा मिलनी चाहिए। क्योंकि इस प्रतिपादन ने पिछले लंबे समय से मनुष्य को दिशा देने और सेवा साधना करने की प्रशस्ति पाई है। इसी दृष्टि से उस समुदाय विशेष के लिए पूर्वजों की थाती को सुरक्षित और जीवंत रखने का धर्म कर्तव्य पालन करने का विशेष दायित्व माना जाता है।
निष्पक्ष विवेक, विश्व, विवेक का कर्तव्य है कि देव संस्कति की गरिमा और उपयोगिता को बिना झिझके स्वीकारें किंतु, ऐसा करने पर निकटवर्ती लोगों का पूर्वाग्रह बुरा मानेगा। यदि ऐसा अन्यत्र न बन पड़े तो भी इन उत्तराधिकारियों को विशेष रूप से जागरूकता बरतनी चाहिए कि ऐसी महान धरोहर धूमिल न होने पाए जिसने पिछले दिनों मानवता की महान सेवा की है और जिससे भविष्य में विश्व को शांति और प्रगति में महान योगदान मिलने की संभावना है।
कोई बात कितनी ही महान क्यों न हो, यदि वह व्यवहार में न उतरे, चिंतन पर छाई रहे, तो पुस्तकों में सीमाबद्ध रहने पर उपेक्षित होते-होते वह विस्मृति के गर्त में जा गिरेगी और अपना अस्तित्व गँवां देगी।
‘संस्कृति’ दर्शन व परंपरा का एक समुच्चय है। अध्यात्म और धर्म का जोड़ा है। अध्यात्म आस्था को एवं व्यवहार को कहते हैं। मान्यताएँ क्रियाकलापों में भी उतरनी चाहिए। देवसंस्कृति के अनुयायी चाहे वे भारत में बसे हों अथवा प्रवासियों के रूप में सुदूर देशों में, उनका यह कर्तव्य है कि यदि वे उसकी गरिमा को स्वीकार करते हैं तो इतना और करें कि उनके आहार-विहार प्रथा प्रचलन रीति-रिवाज, कला-सज्जा, संभाषण, शिष्टाचार आदि में भी उसकी झलक दिखा सकें।
पश्चिम को प्रगतिशील मानना हो और उनका अनुकरण करना हो तो इस तथ्य पर भी गौर करना चाहिए कि वे अपनी संस्कृति को ईसाई धर्म से अधिक प्यार करते थे। गर्म देशों में रहते हुए भी ठंडे मुल्कों की पोशाक पहनने में वे अपना गौरव मानते थे। संस्कृति की अवधारणा एवं निर्वाह आत्म गौरव का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
संसार का सामान्य क्रम प्रकृति-प्रेरणा के अनुरूप चल रहा है। प्राणी समुदाय की चेष्टाएँ उसी ढर्रे में गतिशील रहती हैं। पर मनुष्य की स्थिति अन्य सभी प्राणियों से भिन्न है। यह कर्म प्रधान है, उच्चस्तरीय पुरुषार्थ संपन्न प्राणी हैं। विकास की असीम संभावना होते हुए भी मनुष्य के शरीर में वासना, मन में तृष्णा तथा अंतराल में अहंता और वातावरण में निकृष्टता, प्रचलन में पशु-प्रवृत्तियों का बाहुल्य रहने से खतरा यह बना रहता है कि मानवी गरिमा असुरता के चंगुल में फँसकर कहीं उस देवोपम सौभाग्य को दुर्भाग्य में न बदल दें। प्रगति की संभावनाओं से वह विमुख न हो जाए। आकर्षणों के जाल-जंजाल में फँसकर कहीं सुरदुर्लभ सुयोग को नरक की संरचना में न लगा बैठे।
पतनोन्मुखी प्रवाह से बचकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने तथा उन महान संभावनाओं को साकार कर सकने के लिए अभीष्ट परिणाम में साहस एवं विवेक का होना आवश्यक है। इन गुणों के सहारे एकाकी अपने बलपूते प्रगति पथ की ओर बढ़ सके इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा चाहिए। ऐसी शिक्षा जो मानव के संचित कुसंस्कारों को दबाने तथा प्रसुप्त दैवी तत्त्वों को उभारने में समर्थ हो सके, यह संस्कृति कहलाती है। संस्कृति अर्थात् व्यक्तित्व को परिष्कृत तथा सुविकसित करने वाली विद्या। इसके दार्शनिक पक्ष को अध्यात्म और व्यवहार को धर्म कहते हैं। दोनों के समन्वय से परिपूर्ण स्तर की जीवन शिक्षा की व्यवस्था बनती है। चिंतन और स्वभाव में उतरकर वह जीवन विद्या मनुष्य को महान बनाती है। ऐसी विशेषताओं से सुसंपन्न मनीषियों को सांसारिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर पाते। संसार के पतनोन्मुख प्रवाह की उल्टी दिशा में वे मछली की भांति धार को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book